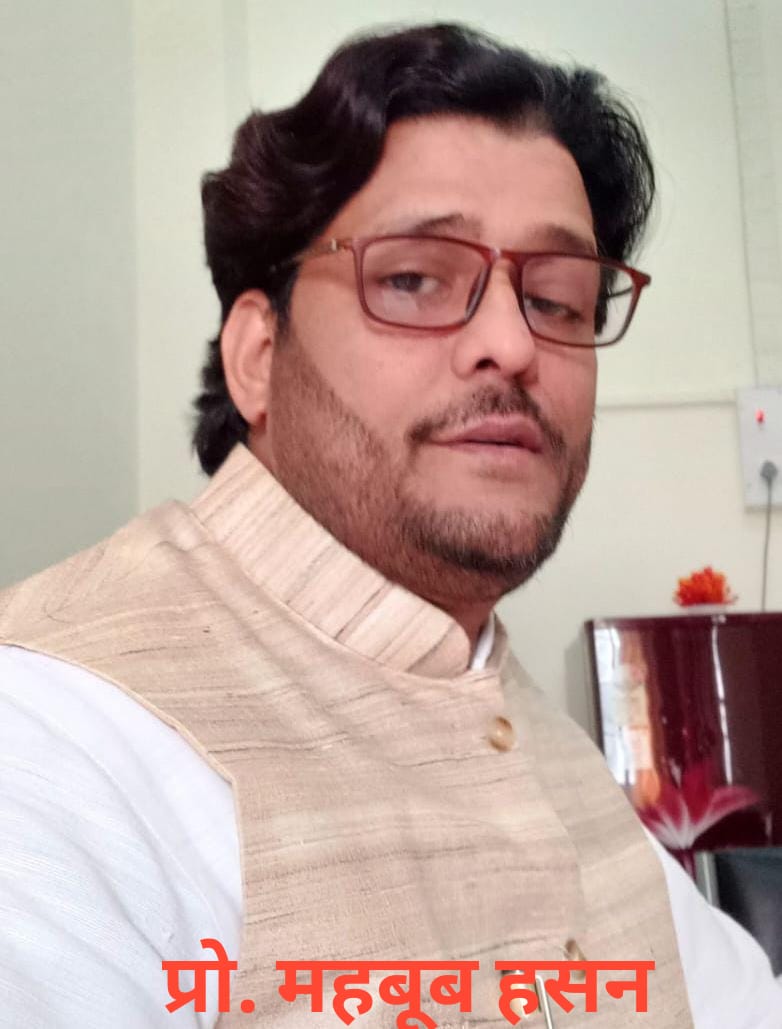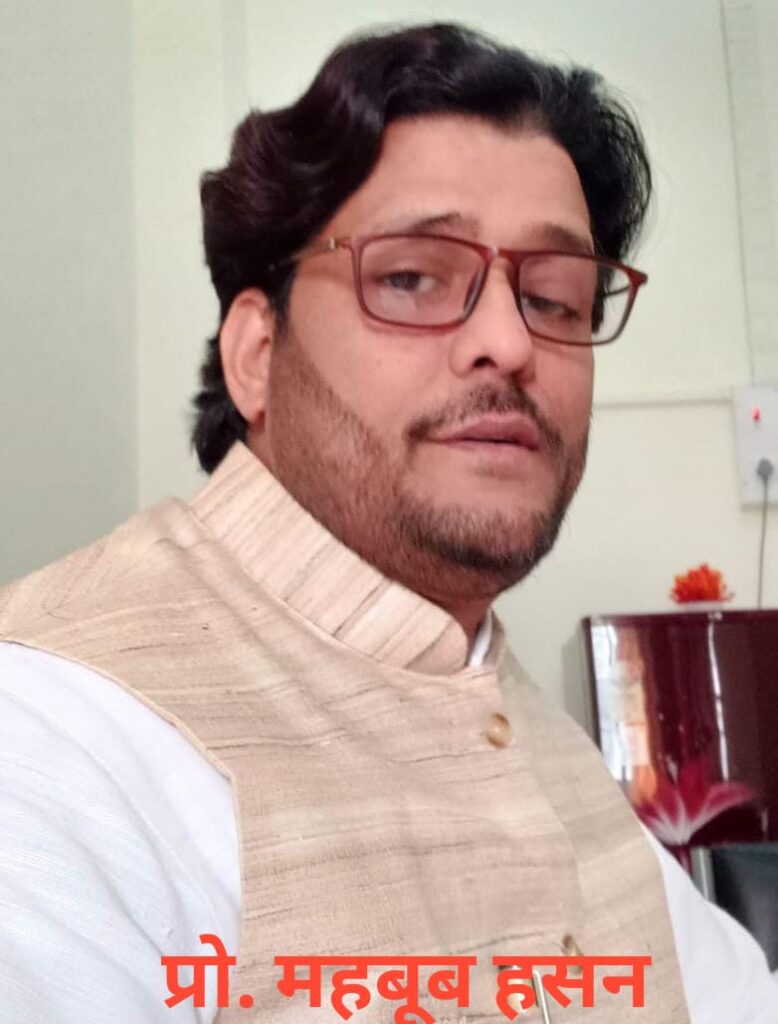
- प्रो. महबूब हसन
भारत सांस्कृतिक، धार्मिक और भाषाई विविधता एवं समरसता का देश है। यहाँ हज़ारों किस्म की जबानें और बोलियां प्रचलित हैं। हमारी परंपराओं में विभिन्न प्रकार के धर्म-संप्रदाय, रंग-नस्ल, रीति-रिवाज, वेश-भूषा और आहार-व्यवहार शामिल हैं। सभी की अपनी अपनी प्रासंगिकता और मान्यताएं हैं। उन तमाम विविधताओं से मिल कर ही हिन्दुस्तान बनता है और यही खूबियां इस देश को महान बनाती हैं। अनेकता में एकता की ये खूबसूरत मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। दर असल हमारा मुल्क एक ऐसे खूबसूरत चमन की मानिंद है, जिस में रंग-रंग और भांति भांति के फूल खिले हों। किसी शायर ने क्या खूब कहा है:
चमन में इख़्तिलात-ए-रंग-ओ-बू से बात बनती है
हम ही हम हैं तो क्या हम हैं तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो
भाषाएं और बोलियां अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती हैं। भाषाएं सामाजिक रिश्तों का ताना-बाना भी तैयार करती हैं। भाषा और साहित्य के बग़ैर एक आदर्श समाज की कल्पना संभव नहीं। ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। ज़बान के पैदा होने और फलने-फूलने की एक लंबी दास्तान होती है। इंसानों की तरह ज़बानों के भी खानदान होते हैं। भाषाविदों के मुताबिक भाषाएं और बोलियां इंसानों की तरह पैदा होती हैं और अपनी उम्र गुज़ार कर शिथिलता का शिकार भी होती हैं। उर्दू एक बेहद लोकप्रिय भाषा रही है। कभी उर्दू को हिंदी, हिंदवी और रेख़्ता के नाम से भी जाना पहचाना गया। इन नामों से भी उर्दू की भाषाई और सांस्कृतिक उदारता प्रकट होती है। इसे चाहने वालों की संख्या में हर रोज़ इज़ाफ़ा हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनियां में तक़रीबन 230 मिलियन लोग उर्दू बोलते हैं। इस ज़बान का जन्म हिंदुस्तान की मिट्टी में हुआ। इस की पैदाइश की कहानी 12 वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रीय अपभ्रंश से शुरू होती है। उर्दू ज़बान के पास इस मिट्टी की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर की एक शानदार विरासत मौजूद है।
उर्दू अमन और मुहब्बत की ज़बान है। उर्दू रिश्तों की तुरपाई करती है। रिश्तों में मिठास घोलती है। बशीर बद्र ने क्या खूब कहा है “सात संदूक़ों में भर कर दफ़्न कर दो नफ़रतें/आज इंसाँ को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत” मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने कहा था “अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो इश्क़ कर लीजिए और अगर इश्क़ करना चाहते हैं तो उर्दू सीख लीजिए” मीर, ग़ालिब और फिराक ने अपनी ग़ज़लों में इश्क़ के मुख्तलिफ रंग-ओ-रूप को कलात्मक अंदाज में चित्रित किया है। उन की रचनाओं में माशूक के हुस्न-ओ -जमाल के साथ साथ रूह में उतर जाने की आरज़ू भी है। इश्क़-ओ-मुहब्बत के साथ साथ उर्दू इंकलाब और कुर्बानी का संदेश भी देती है। पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, फैज़, जोश और इक़बाल की नज़्मों में वतन परस्ती का जज़्बा कूट कूट कर भरा है। चकबस्त की नज़्म “ख़ाक-ए-हिन्द” में मुल्क के प्रति समर्पण/कुर्बानी का पैग़ाम देती है। इक़बाल की नज़्म “तराना-ए-हिन्दी” (सारे जहाँ से अच्छा) देशभक्ति की उम्दा मिसाल है। ये नज़्म हिंदुस्तान की अज़मत/महानता को भावपूर्ण अंदाज में पेश करती है। उन एक दूसरी नज़्म “नया शिवाला” की पंक्ति “ख़ाक-ए-वतन का मुझ को हर ज़र्रा देवता है” मुल्क की मिट्टी के प्रति गहरा प्रेम एवं सम्मान व्यक्त करती है। देशभक्ति में डूबी हुई उर्दू की बेशुमार ऐसी काव्यगत रचनाएं हैं, जिन में देश के लिए श्रद्धा एवं अक़ीदत का जज़्बा झलकता है। उर्दू ने स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। “इंकलाब जिंदाबाद” का नारा आज़ादी के मतवालों का लहू गर्म करता रहा। मशहूर उर्दू ग़ज़ल “सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है/देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है” हमारे अंदर देश पर मर मिटने का जज़्बा पैदा करती है। स्वतंत्रता संग्राम के पहले पत्रकार मौलवी मुहम्मद बाकर(1780-1857) को ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के जुर्म में तोप से उड़ा दिया था। ये बात फख्र के साथ कही जा सकती है कि शायरी, फिक्शन और उर्दू पत्रकारिता ने आजादी की लड़ाई में अविस्मरणीय भूमिका अदा की है।
उर्दू भाषा और साहित्य को सींचने और संवारने में विभिन्न मज़हब/संप्रदाय के अदीबों और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अफ़सोस कि उर्दू को एक ख़ास मज़हबी तबके से नत्थी किया जाता है। जबकि उर्दू सभी को गले लगाती है। उर्दू साहित्य का पहला इतिहास राम बाबू सक्सेना ने लिखा। उर्दू की पहली ग़ज़ल चंद्रभान ब्राह्मण ने रची। अमीर खुसरो से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक बहुत से क़लम कारों ने इस साझी विरासत को समृद्ध किया। इंशा अल्ला खां इंशा की उत्कृष्ट रचना “रानी केतकी की कहानी” उस साझी विरासत की महत्वपूर्ण कड़ी है। ऊर्दू कथा साहित्य को गति देने में मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, रामानंद सागर, उपेन्द्र नाथ अश्क, राजेंद्र सिंह बेदी, जोगेंद्र पाल, सुरेन्द्र प्रकाश, रतन सिंह जैसे नामचीन गैर मुस्लिम रचनाकारों ने अहम भूमिका निभाई। उर्दू शायरी की दुनियां में पंडित दयाशंकर नसीम, पंडित बृज नारायण चकबस्त, जगन नाथ आज़ाद, त्रिलोक चंद महरूम, फ़िराक़ गोरखपुरी और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी वगैरह का नाम सम्मान से लिया जाता है। पंडित दयाशंकर नसीम(1811–1845) का शुमार लखनऊ के प्रमुख शायरों में होता है। उन की मसनवी(महाकाव्य) “गुलज़ार-ए-नसीम” के बग़ैर उर्दू साहित्य का इतिहास अधूरा है। ये महाकाव्य लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट की प्रतिनिधि रचना है। अनूठी शैली एवं शिल्प में रचित कृति “गुलज़ार-ए-नसीम” तमाम विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस महाकाव्य के बारे चकबस्त ने लिखा है कि “पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी की शक्ल में मोती पिरोए हैं” इस ज़बान के कंपोजिट कल्चर को समृद्ध करने वाले सभी ग़ैर मुस्लिम-क़लम कारों पर ऊर्दू को हमेशा नाज़ रहेगा।
उर्दू की ऐतिहासिक पत्रिका “ज़माना” के संपादक दयानारायण निगम (1882 -1942) का योगदान उर्दू साहित्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने ने मासिक पत्रिका “ज़माना” के माध्यम से उर्दू भाषा और साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की। प्रेमचंद की पहली कहानी “‘दुनिया का सबसे अनमोल रतन” और अल्लामा इक़बाल की सुप्रसिद्ध नज़्म “सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा” पहली बार इसी मैगज़ीन में प्रकाशित हुई थी। नवाबराय के नाम से लिखने वाले धनपतराय को प्रेमचन्द का नाम दयानारायण निगम ने दिया था। उर्दू की साझी विरासत के संदर्भ में मुंशी नवल किशोर(1936-1985) को नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। मुंशी नवल किशोर का जन्म एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उर्दू भाषा और साहित्य पर उन के बड़े उपकार हैं। उन्होंने ने अपने नाम से प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। उत्तर भारत का पहला उर्दू समाचार पत्र “अवध अख़बार” नवल किशोर प्रेस से ही शुरू हुआ। मिर्ज़ा ग़ालिब जैसे महान शायर की रचनाएं और कृतियां इसी प्रेस से प्रकाशित हुईं। मिर्ज़ा ग़ालिब ने अपने एक खत में लिखा है “इस प्रेस ने जिसका भी दीवान(संग्रह) छापा, उसको ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया” नवल किशोर प्रेस से उर्दू के अलावा अंग्रेजी, हिंदी संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, मराठी, बंगाली और गुरुमुखी आदि भाषाओं की हज़ारों किताबें प्रकाशित हुईं। इस अवसर पर उर्दू, अरबी और फारसी के प्रचंड विद्वान मालिक राम (1906-1993) का जिक्र भी लाज़मी है। उन की महत्वपूर्ण किताब “तज़किरा-ए-मुआसरीन” के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन का शुमार ग़ालिब के चुनिंदा आलोचकों और विशेषज्ञों में होता है। उन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने पसंदीदा शायर मिर्ज़ा ग़ालिब के अध्ययन में लगाया। ग़ालिब के हवाले से उन की किताब “ज़िक्र-ए-गालिब” “फसाना-ए-ग़ालिब” और “तलामिज़ा-ए-ग़ालिब” को आज भी आधिकारिक हैसियत हासिल है। मालिक राम ने मिर्ज़ा ग़ालिब की उर्दू व फ़ारसी कृतियों “दीवान-ए-ग़ालिब” “सब्द-ए-चिन” “गुल-ए-राना” और “ख़ुतूत-ए-ग़ालिब” का संपादन भी किया।
उर्दू की साझी विरासत के क्रम में प्रो. गोपीचंद नारंग (1931-2022) का नाम गर्व के साथ लिया जाता है। प्रो. नारंग का शुमार उर्दू के शीर्ष विद्वानों में होता है। प्रख्यात विचारक, आलोचक और भाषाविद के तौर पर गोपीचंद नारंग ने उर्दू साहित्य जगत में उत्तर आधुनिकतावाद की नींव रखी। पोस्ट मॉडरिज्म के जनक के तौर पर उन्होंने ने उर्दू में नए नए साहित्यिक विमर्श पैदा किए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे। बेशुमार महत्वपूर्ण किताबें लिखीं। पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इक़बाल सम्मान, ग़ालिब पुरस्कार, सर सैयद एक्सीलेंस पुरस्कार जैसे अहम सम्मान से नवाजे गए। पाकिस्तान ने उन्हें सितार-ए-इम्तियाज़ और राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से अलंकृत किया। साहित्य अकादमी और राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली जैसी बड़ी संस्थाओं के चेयरमैन रहे। उन्होंने कई देशों में उर्दू भाषा और साहित्य की नुमाइंदगी की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गोपी चंद नारंग के साहित्यिक योगदान पर शोध कार्य जारी हैं। उन के व्यक्तित्व और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
देश की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में ज़बानों का आपसी रिश्ता क़ाबिल-ए-ग़ौर है। भाषाएं और बोलियां अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का आईना भी होती हैं। सांस्कृतिक समरसता की बुनियाद पर उर्दू को हिंदी की सगी बहन कहा गया है। दोनों में ग़ज़ब की समानताएं हैं। लिपी से इतर दोनों का व्याकरणिक संरचना काफी समान है। खड़ी बोली से दोनों का गहरा नाता है। दुनियां की किसी भी दो ज़बानों में इतनी समानताएं नहीं मिलतीं। उर्दू और हिंदी का भाषाई संबंध सांझी विरासत की खूबसूरत मिसाल है। जहां एक तरफ़ ग़ैर मुस्लिम रचनाकारों ने उर्दू भाषा और साहित्य की उत्कृष्ट सेवा की वहीं दूसरी तरफ अमीर खुसरो, अब्दुर्रहीम खानखाना, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, राही मासूम रजा, मंजूर एहतेशाम और अब्दुल बिस्मिल्ला जैसे मुस्लिम साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का संस्कृत से गहरा संबंध है। उपर्युक्त दोनों जबानें इंडो-आर्यन भाषा परिवार से हैं। अर्थात संस्कृत से प्राकृत भाषाएँ वजूद में आईं और फिर उनसे उर्दू और हिंदी जैसी आधुनिक जबानें पैदा हुईं। दर असल संस्कृत एक ऐसी प्राचीन ज़बान है, जिस ने मुख्तलिफ इंडो-आर्यन भाषाओं को प्रभावित किया। इसी लिए संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा गया है। उर्दू फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है लेकिन उत्पत्ति, व्याकरण और शब्दावली के दृष्टिकोण से इस का रिश्ता संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं से जुड़ता है। उर्दू में प्रचलित संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कहावतों और और मुहावरों का अधिकांश हिस्सा संस्कृत और हिंदी से लिए गए हैं। भाषाविदों के अनुसार उर्दू ने अवधि, हरियाणवी, बुन्देली, कन्नौजी, पंजाबी, बंगाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का असर भी कुबूल किया। ऊर्दू की ये विशेषताएं उस की भाषाई समरसता को दर्शाती हैं।
दुनियां की हर ज़बान अपने मुल्क की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और धार्मिक सभ्यता एवं संस्कृति को प्रमुखता से व्यक्त करती है। उर्दू हिंदुस्तान की एक ऐसी लोकप्रिय ज़बान है, जो अपनी मिट्टी की ख़ुशबू और मुल्क की तहज़ीबी रंगारंगी को खुद में समेटे हुए है। 18 वीं सदी के जनकवि नज़ीर अकबराबादी की कृतियां हिंदुस्तान की गंगा-जमुनी तहज़ीब, सामाजिक जीवन, मेले ठेले और यहां की दूसरी सांस्कृतिक विविधता का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती हैं। उर्दू रचनाओं में अगर ईद और शब-ए-बारात की खुशियां नज़र आती हैं तो होली एवं दीवाली का उल्लास भी मौजूद है। हैदर बयाबानी, जोश मलीहाबादी, कैफ़ी आज़मी और नज़ीर बनारसी, निदा फ़ाज़ली और जावेद अख्तर वगैरह की कृतियों में हिंदू तीज त्योहारों का भावपूर्ण वर्णन मिलता है। नज़ीर अकबराबादी की नज़्म “दीवाली” की चार पंक्तियां पेश-ए-खिदमत हैं:
हर इक मकाँ में जला फिर दिया दिवाली का
हर इक तरफ़ को उजाला हुआ दिवाली का
सभी के दिल में समाँ भा गया दिवाली का
किसी के दिल को मज़ा ख़ुश लगा दिवाली का
उर्दू ज़बान में वेद, रामायण, महाभारत और गीता की दर्जनों अनुवादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वेद हिंदू धर्म का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। उर्दू में वेद के कई अनुवाद उपलब्ध हैं। उर्दू के बड़े शायर अनवर जलालपुरी ने गीता का तर्जुमा उर्दू शायरी में किया है। चकबस्त ने रामायण जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक महाकाव्य को उर्दू का लिबास पहनाया। अखिल भारतीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली ने रामायण, महाभारत और गीता के उर्दू अनुवाद प्रकाशित किए हैं, जिसके फलस्वरूप उन धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जीवन दर्शन उर्दू भाषी लोगों तक सुगमता से पहुंच सका। उर्दू का ये समावेशी मिज़ाज उसे समरसता और विविधता प्रदान करता है। उर्दू साहित्य में हिंदी देवी-देवताओं और सूफ़ी-संतों का श्रद्धापूर्वक उल्लेख किया गया है। उर्दू शायरी में कृष्ण-भक्ति का खूबसूरत अक्स उभरता है। शायरों ने कृष्ण के मुख्तलिफ रूप को पेश किया है। प्रगतिशील शायर हसरत मोहानी को कृष्ण से खास अक़ीदत थी। जन्माष्टमी के अवसर पर हसरत मोहानी अक़ीदत के साथ मथुरा हाज़िरी देते थे। उन का शेर है: हसरत की भी क़बूल हो मथुरा में हाज़िरी/सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है ख़ास। श्री रामचन्द्र के जीवन, आदर्श और उन की भक्ति पर आधारित उर्दू में कई नज़्में लिखी गई हैं। इक़बाल ने अपनी सुप्रसिद्ध नज़्म “राम” में मर्यादा पुरुषोत्तम की अज़मत पर रोशनी डालते हुए लिखा है:
इस देश में हुए हैं हज़ारों मलक सरिश्त
मशहूर जिन के दम से है दुनिया में नाम-ए-हिंद
है राम के वजूद पे हिन्दोस्ताँ को नाज़
अहल-ए-नज़र समझते हैं उन्हें इमाम-ए-हिन्द
भारत की सांस्कृतिक परंपरा के प्रति उर्दू का रवैया बेहद सकारात्मक रहा है। अपने प्रगतिशील विचार एवं विमर्श के आधार पर उर्दू ने सदैव मानवता, भाईचारा और सौहार्द्र जैसे मानवीय मूल्यों की हिमायत की है। उर्दू साहित्य ने सभी सामाजिक और धार्मिक तबकों के प्रति उदारता का परिचय दिया है। शायरों और अदीबों ने सांप्रदायिक और धार्मिक संकीर्णता एवं आडंबर का मज़ाक उड़ाया है। ख़्वाजा हैदर अली आतिश का मशहूर है “बुत-ख़ाना खोद डालिए मस्जिद को ढाइए/दिल को न तोड़िए ये ख़ुदा का मक़ाम है” हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होने और फलने-फूलने वाली उर्दू पूर्ण रूप से सेक्युलर भाषा है। इस का क्रमिक विकास विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के प्रभाव से हुआ है। इस लिए ऊर्दू ज़बान को सांझी विरासत का प्रतीक कहना मुनासिब होगा।
संजीव सराफ द्वारा स्थापित रेख़्ता फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू का झंडा बुलंद कर रहा है। 2012 में स्थापित रेख़्ता फाउंडेशन उर्दू भाषा एवं साहित्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व समृद्ध करने के लिए समर्पित है। रेख़्ता की वेबसाइट पर उर्दू की तक़रीबन पांच लाख ई-बुक्स मौजूद हैं। जश्न-ए-रेख़्ता के नाम से नई दिल्ली में हर साल तीन दिवसीय प्रोग्राम होता है। इस अवसर पर तरह तरह के साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। खुशी की बात है कि समकालीन समय में भी उर्दू के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। आशा है कि उर्दू की सांस्कृतिक विरासत का ये सफर निरंतर जारी रहेगा।
(लेखक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में
उर्दू के सहायक आचार्य हैं)